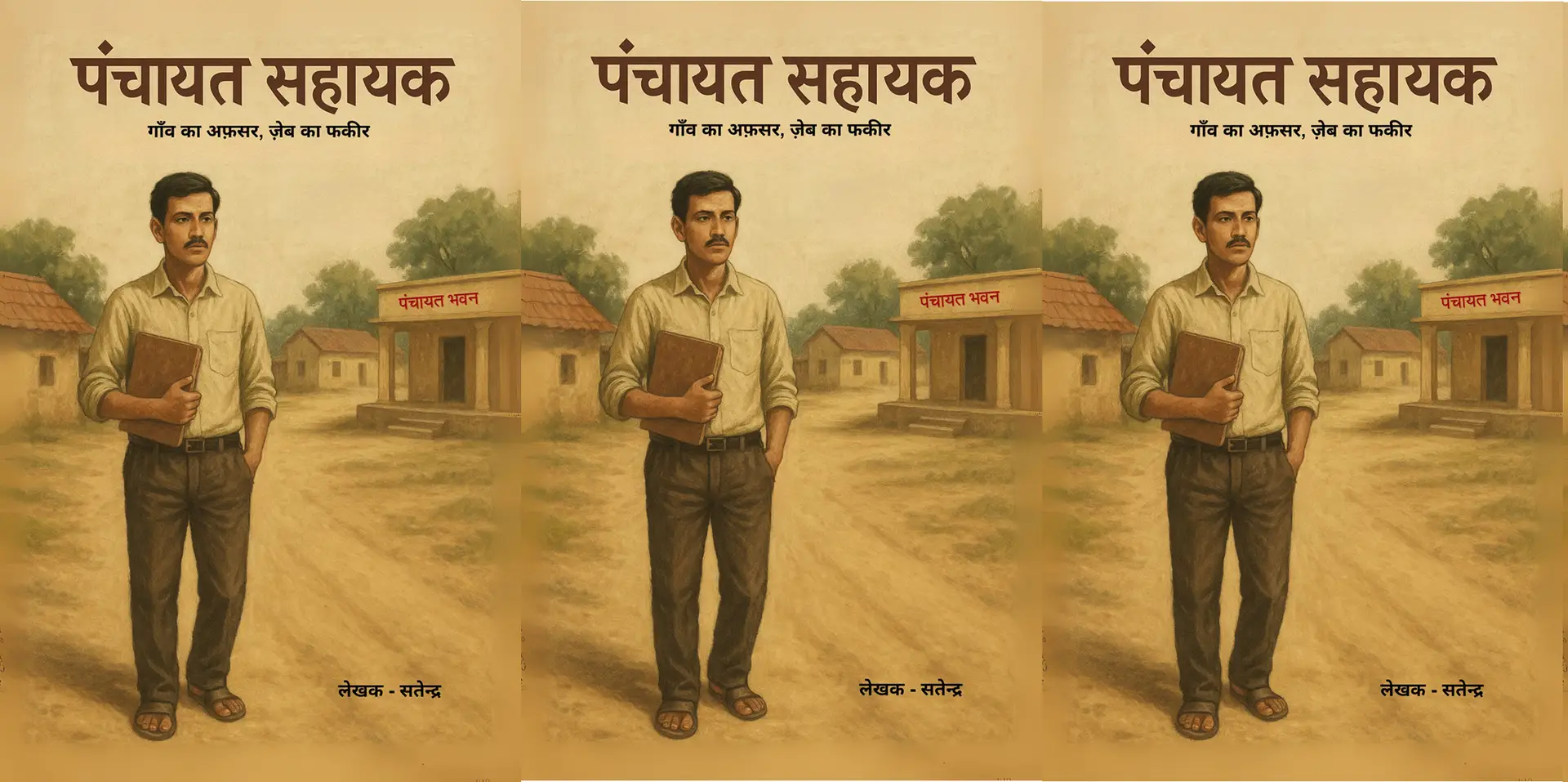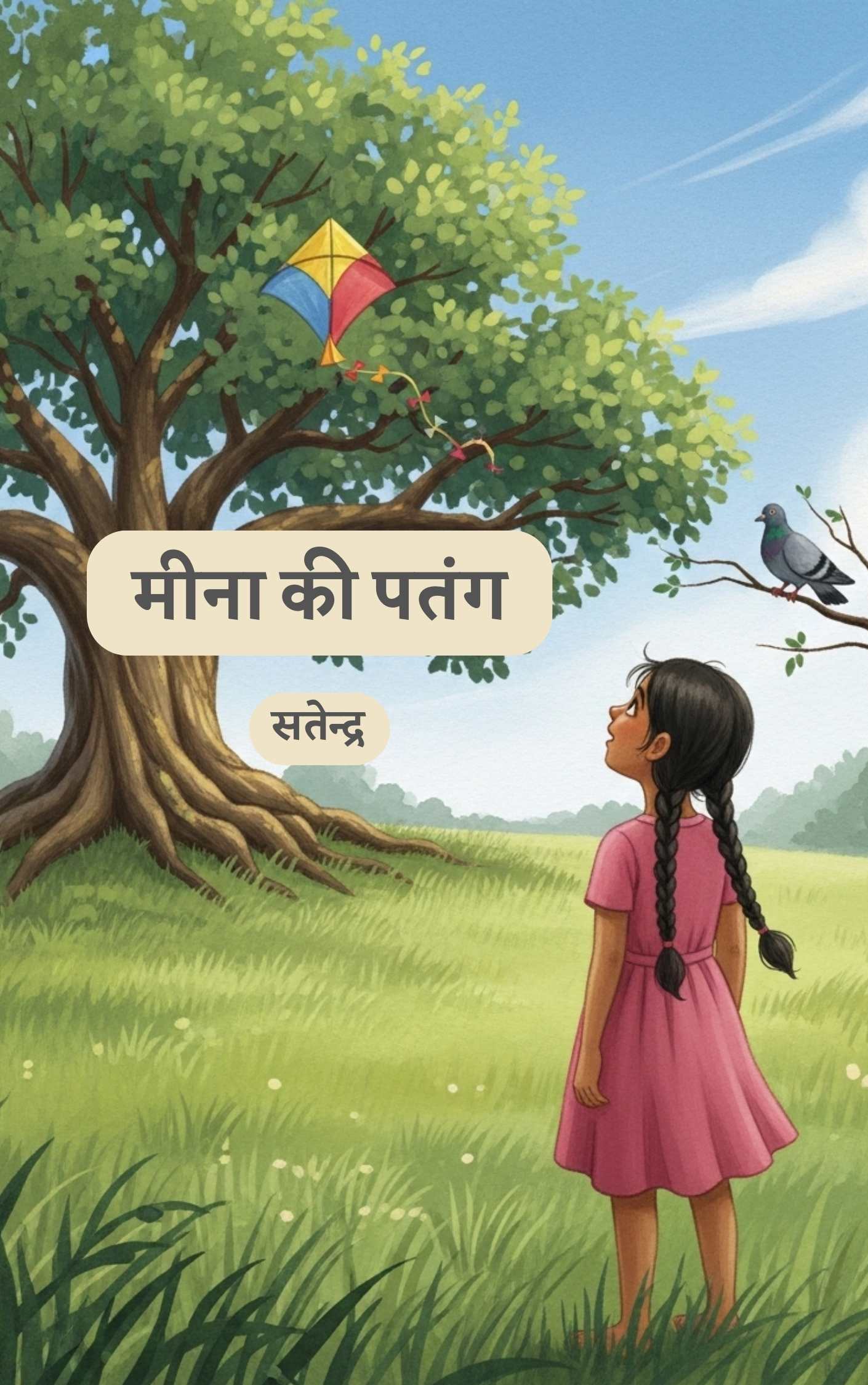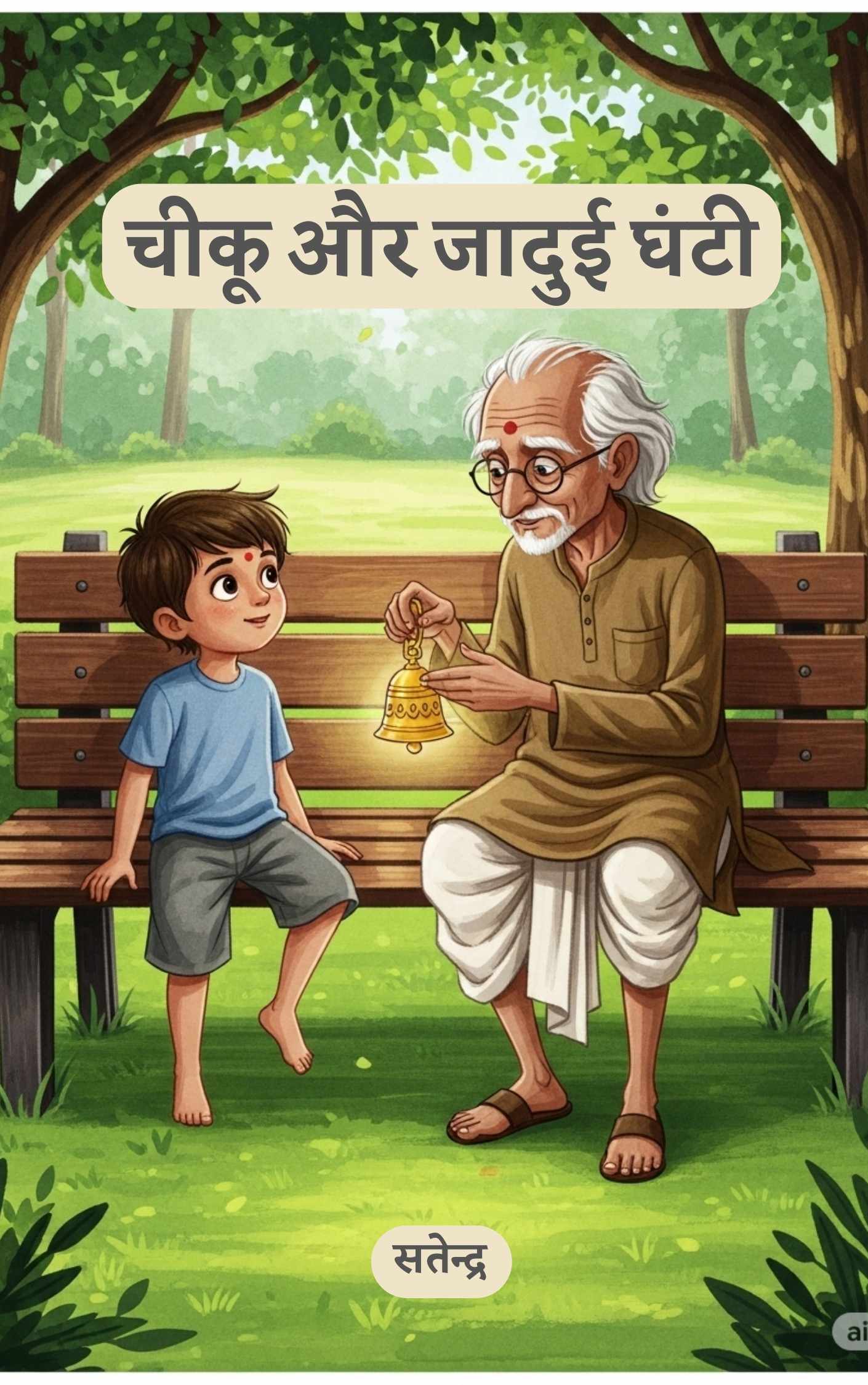नमस्कार आज पढिये युवा लेखक सतेन्द्र का लिखा प्रथम उपन्यास पंचायत सहायक – गांव का अफसर, जेंब का फ़कीर। लेखक सतेन्द्र जिला बदायूँ उत्तर प्रदेश के छोटे से कस्बे सिमरिया के रहने वाले है जोकि वर्तमान में पंचायत सहायक के पद पर कार्यरत है। सतेन्द्र का कहना है कि यह उपन्यास केवल एक कहानी नहीं बल्कि उस स्याही की गवाही है, जो मैंने अपने भावों को ह्रदय से निचोड़कर निकाली है। गाँव-गाँव घूमते हुए, पंचायत भवनों की खामोश दीवारों से महसूस किए, मैंने विवेक (उपन्यास का मुख्य किरदार) जैसे हजारों पंचायत सहायकों के दिलों की चीखें सुनीं, जिनके हाथों में सरकारी मुहर तो है, पर भविष्य के पन्ने अब भी खाली हैं।
यह उपन्यास उन सभी पंचायत सहायकों की पीड़ा को व्यक्त करता है जो हर दिन एक उम्मीद और अपमान के बीच झूझते हैं और व्यवस्था के बोझ के नीचे दबकर भी ईमानदारी की साँस लेते हैं। मेरी प्रार्थना है कि यह रचना आप पाठकों को सिर्फ एक कहानी न लगे, बल्कि एक ऐसे सत्य का अहसास कराये— जो आज भी अनसुना है। मेरे शब्दों में माँ के संस्कार है और हिम्मत में पिता की परछाई मैं उनके बिना कुछ भी नहीं। मेरा उनको कोटि कोटि प्रणाम। तो चलिए अब आपको ले चलते है सतेन्द्र के इस अनसुने सफ़र पर।
अध्याय 1 – एक अफ़सर की अधूरी कहानी
घड़ी की टिक-टिक रात भर विवेक की नींद चुराती रही। कमरे में बस सन्नाटा था, जहाँ दीवार पर टँगा हुआ एक पुराना कैलेंडर मौन खड़ा था, और बगल में टँगी नेहा की एक हल्की मुस्कान भरी तस्वीर जो अब भी उसके बीते दिनों की कहानी कहती थी। उस तस्वीर की मुस्कान जैसे उसकी बेचैनी की चुप साक्षी बन गई हो।
विवेक की माँ सरस्वती देवी तुलसी में पानी डाल रही थीं, उनके हाथों में थकान थी और आँखों में दुआएँ। हर बूँद जो तुलसी पर गिरती मानो विवेक के रास्तों को आसान करने की प्रार्थना बन जाती।
आँगन में विवेक की बहन चाँदनी, झाड़ू से फर्श बुहारती, लेकिन नज़रें उन किताबों पर अटक जातीं जिन्हें कभी वक़्त नहीं मिला— न पढ़ने का, न जीने का।
भीतर बैठा विवेक पूजा करता है फिर माँ के पैर छूता है और कोने से उठाता है अपना अफ़सराना बैग। एक पुराना ब्राउन सरकारी फाइल बैग, जो अब उसकी पहचान बन चुका है।
उस बैग में समाई होती है एक पूरी जिम्मेदारियों की दुनिया— सरकारी फॉर्म, कुछ ज़रूरी दस्तावेज़, एक निजी डायरी और कुछ नीली-लाल स्याही वाले कलम।
हर चीज़ जैसे उसकी ज़िम्मेदारी की गवाही देती हो। वह अपनी टीवीएस स्पोर्ट बाइक के पास पहुँचता है— जिसे उसने किस्तों पर खरीदा था, हर एक किस्त मानो कुर्बानी। रास्ते में 50 रूपए का पेट्रोल डलवाता है और मन में उठता है वही डर, “कहीं रास्ते में बंद न हो जाए…” लेकिन फिर भी वो चल पड़ता है।
कंधे पर टँगा सरकारी बैग, सीने में उम्मीदें, और आँखों में वो सपना जिसे सिर्फ वही देखता है। यह कहानी अब शुरू हो चुकी है… एक अफ़सर की, जिसकी पहचान सिर्फ उसके बैग में नहीं, जिम्मेदारी में है।
अध्याय 2 – अफ़सर सरकारी, बस नाम का
सूरज सिर पर चढ़ आया था। जून की गर्म दोपहर, तपती सड़कें और उड़ती धूल… अफ़सर विवेक का चेहरा इन सबका मूक गवाह बना खड़ा था। उसने माथे का पसीना रुमाल से पोंछा और अपनी पुरानी टीवीएस स्पोर्ट को ब्लॉक परिसर के बाहर खड़ा कर दिया।
कंधे पर टँगा था उसका बैग— वो बैग, जो न पूरा उसका था, और न पूरी तरह सरकारी पर उसमें बंद थी उसकी पूरी दुनिया… कागज़ों की, सपनों की, जिम्मेदारियों की।
लोहे का गेट धीमे से चरमराया। गार्ड ने घूरकर देखा और ताना मारा— “अबे पंचायत सहायक है ! क्या तू? बड़ी देर कर दी आज !” विवेक मुस्कराया, जैसे ऐसे तानों की आदत हो चुकी हो।
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो उसी सरकारी गंध से टकराया— फाइलों की बासी खुशबू, धूल की परतें और थकी हुई दीवारें।
एक ऐसा सिस्टम, जो सालों से वहीं खड़ा था— जड़, बेजान और बोझिल।
कमरे के भीतर सचिव रमेश दुबे, मोबाइल में खोए हुए, चाय के कुल्हड़ से घूँट भरते हुए बोले—
“आ गए महामहिम पंचायत सहायक ! चलिए, ये फाइलें ले जाइए गाँव और सुनिए, अगले सप्ताह ग्राम सभा है— रिकॉर्ड पूरा तैयार रखना, प्रधान जी का नया प्लान भी टाइप करना है और एक वर्क ऑर्डर बनाना है… वो जो नाली बनी थी…”
विवेक ने धीरे से कहा
“सर… वो तो बनी ही नहीं।”
दुबे जी ने भौंहें चढ़ाईं—
बनी हो न बनी हो… पेपर पर तो बननी चाहिए।
उसी पल दरवाज़ा धड़ाम से खुला। गुटखे की गंध के साथ प्रधान बलबीर सिंह कमरे में दाखिल हुआ। एक हाथ में मोबाइल, दूसरे में दबंगई।
“विवेक ! तू बहुत पढ़ा-लिखा बनता है रे ! ज़्यादा ईमानदारी न झाड़, वरना किसी केस में फँसा दूँगा और नौकरी जायेगी सो अलग, पंचायत सहायक है… लगता है कोई मंत्री बन गया है!”
विवेक खामोश रहा। उसकी आँखों में एक सवाल धधक रहा था—
“क्या यही सरकारी नौकरी है? जिसके लिए मैंने सब कुछ दाँव पर लगा दिया।”
बैग धीरे-धीरे भारी होने लगा था। उसने एक-एक करके सभी फॉर्म निकाले— मनरेगा की लिस्ट, परिवार रजिस्टर, आयुष्मान कार्ड की रिपोर्ट… हर दस्तावेज़ किसी सरकारी योजना का हिस्सा था पर उनमें कहीं विवेक का नाम नहीं था बस एक ‘कर्मचारी’ था।
वेतन बस छः हज़ार रूपये महीना, कब मिला था, याद नहीं। अब कब आएगा? किससे पूछें, सिस्टम भी खामोश है… विवेक ने अपनी डायरी के कोने में लिखा—
“रोज़ काम करता हूँ, रोज़ खुद को खोता हूँ। सम्मान की जगह उपेक्षा मिलती है और हर अफ़सर मुझे नौकर समझता है, क्या वाकई मैं सिर्फ एक नौकर हूँ या फिर एक बेजान अफ़सर— जो सिर्फ कलम घिसता है।”
शाम ढल चुकी थी। विवेक बाहर निकला। पसीने से भीगा, थका और बैग के भार से झुका हुआ और फिर चलते-चलते, मन में एक अंतिम विचार कौंधा—
“मैं अफ़सर तो हूँ… बस नाम का। असल में तो एक मोमबत्ती हूँ—
जो खुद जल रहा है… और रौशनी किसी और को दे रहा है।”
अध्याय 3 – किताबों के बीच छुपी मोहब्बत
रात के दस बज चुके थे। कमरे की दीवारों पर बल्ब की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। विवेक की आँखों में नींद नहीं, कोई पुरानी यादों का साया था। फाइलें एक ओर धरी थीं— चुपचाप। वो उठा, अलमारी खोली और वहाँ से एक बोसीदा डायरी निकाली…
डायरी से पन्नों की ख़ुशबू नहीं, बल्कि यादें निकल रही थीं।
“कक्षा 6 की पहली सुबह की यादें…”
विवेक के ज़हन में एक पुराना स्कूल उतरने लगा। घंटी बजी थी… और उसी पल वो आई, नेहा।
नेहा— वो लड़की जो ज़्यादा बोलती नहीं थी लेकिन उसकी मुस्कान में किताबों से ज़्यादा ज्ञान था। सफ़ेद यूनिफॉर्म, दो चोटियाँ, आँखों में सादगी और आवाज़ में मिठास। विवेक हमेशा पीछे की बेंच पर बैठता था और नेहा सबसे आगे। जब भी टीचर सवाल पूछते, नेहा जवाब देती…और विवेक उसे निहारता—
हर जवाब पर थोड़ा और सीधा बैठने लगता।
एक दिन नेहा ने पलटकर पूछा—
“तुम्हारे पास हिंदी की किताब है, क्या? मेरी छूट गई घर पर…”
विवेक ने किताब आगे बढ़ा दी— थोड़ा सकुचाया, थोड़ा मुस्कुराया। वहीं से शुरू हुआ वो रिश्ता— बिना नाम का, बिना इजाज़त के, पर हर रोज़ थोड़ा और गहरा होता गया। इंटरवेल में खाने के टिफिन शेयर होने लगे, निजी बातें साझा होने लगी और अक्षरों के साथ-साथ एक दूसरे के दिल भी पहचानने लगे थे। विद्यालय से लौटते बक्त अक्सर दोनों एक ही रास्ते से घर आते।
नेहा कभी-कभी कहती—
“जब तुम बड़े अफ़सर बन जाओगे, तो मुझे भूल तो नहीं जाओगे न?”
विवेक मुस्कुराता हुआ—
“तुम्हें भूल जाऊं… तो अफ़सर बनने का क्या फ़ायदा !”
लेकिन दुनिया को तो हमेशा कुछ और ही मंज़ूर होता है। नेहा के पिता स्कूल मास्टर थे। सीधे, सख़्त और समाज के कायदे-कानूनों के पक्के।
“लड़की की शादी करनी हो तो लड़का सरकारी अफ़सर ही होना चाहिए और अच्छी तनख्वाह वाला भी, जो थाठ से रख सके मेरी फूल-सी बेटी को।”
नेहा ख़ामोश रहती लेकिन उसकी आँखें हर दिन विवेक को पढ़ती थीं—
उस संघर्ष को, जो सिर्फ किताबों से नहीं, समाज और सिस्टम दोनों से लड़ रहा था।
बारहवीं के बाद, नेहा को कोचिंग के लिए शहर भेज दिया गया। विवेक गाँव में ही रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता रहा। कभी-कभार फ़ोन पर बातें होतीं—
कभी एसएमएस, कभी मिस्ड कॉल… और कभी, सिर्फ इंतज़ार।
फिर एक दिन, विवेक का सपना पूरा हुआ। वह पंचायत सहायक बन गया। खुशी-खुशी उसने नेहा को फोन किया।
फ़ोन किसी और ने उठाया— नेहा के पिता।
“देखो बेटा, अब तुम दोनों की राहें अलग हैं। पंचायत सहायक कोई नौकरी थोड़े ही है… ये तो बस वक़्त काटने का बहाना है।”
विवेक चुप रहा। कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई।
उसने नेहा को आख़िरी मेसेज भेजा—
“नेहा, मैंने तुम्हारे लिए ये नौकरी पायी पर शायद ये तुम्हारे लायक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें वो सब मिले, जो मैं नहीं दे पाउँगा।
मेरी मोहब्बत सच्ची है… लेकिन शायद काफ़ी नहीं।”
उस रात डायरी के एक पन्ने में नेहा का नाम फिर से दर्ज हुआ— किताबों के बीच, यादों के कोनों में।
उसकी एक तस्वीर वो अब भी रखे हुए है—
उन्ही पन्नों के बीच, जहाँ वो ज़िंदगी का मतलब खोजता है।
“नेहा उसकी मोहब्बत थी—
जो उसके पास थी, पर उसकी कभी नहीं हो सकी।”
अध्याय 4 – पंचायत सहायक की जिम्मेदारियाँ
सुबह के सात बज चुके थे। घड़ी की टिक-टिक जैसे विवेक के भीतर चल रही थी। हर एक पल यही दोहरा रहा था—
“इस महीने भी पैसे नहीं बचे…”
चाय के डिब्बे में रखे 120 रूपए, बिजली का बिल टेबल पर पड़ा हुआ और माँ के दवा की पर्ची—
जो माँ ने तकिए के नीचे दबा रखी थी, जैसे बीमारी को कुछ दिनों के लिए चुप बैठने का आदेश दे दिया गया हो।
उस छोटे से घर की दीवारें मिट्टी की थीं, छत टीन की और आँगन में तुलसी का पौधा हवा में लहराता हुआ— जैसे अब भी उम्मीद बची हो।
सरस्वती देवी— गठिया और मधुमेह से पीड़ित माँ, फिर भी सुबह-सुबह रसोई में खड़ी थीं।
“बेटा, दवा खत्म हो गई है… पर तू चिंता मत कर, आज काढ़ा ही पी लूँगी।”
चाँदनी, विवेक की छोटी बहन, सिर झुकाए बोली—
“भैया… मेरी सहेली की अगले महीने शादी है… बाज़ार से मेरे लिए नई चूड़ियाँ ला देना..”
घर की सारी जिम्मेदारी, विवेक के कंधों पर ही तो थी। विवेक की ज़ेब में सिर्फ 120 रूपए थे। उसने कुछ नहीं कहा। सरकारी कागज़ों में विवेक एक ‘कर्मचारी’ था लेकिन उसके बैंक खाते में महीनों से कोई पैसा नहीं आया था। हर बार सचिव रमेश दुबे यही कहते,
“मानदेय फँसा है, ऑर्डर आएगा तो मिलेगा… वित्त विभाग में फाइल अटकी है।” और विवेक वही झूठ घर लौटकर दोहराता।
जिम्मेदारियाँ कई थीं और जो उसे थकने नहीं देती थी। माँ की दवा— 750 रूपए हर महीने,
बहन की पढ़ाई— जो अब सिर्फ एक सपना रह गई थी,
बिजली का बिल— 310 रूपए,
मोबाइल रिचार्ज— ताकि सरकारी कॉल मिस न हो,
पेट्रोल— जैसे विवेक की इज़्ज़त और मोटरसाइकिल दोनों की एक ही टंकी में साँसें चल रही थीं।
“कभी-कभी लगता है ये नौकरी नहीं, किसी की मज़बूरी निभा रहा हूँ मैं…” उसने यही सोचा और चुपचाप निकल पड़ा।
शाम को माँ ने धीरे से कहा, बेटा.. “अब चाँदनी की शादी के लिए रिश्ते देखने चाहिए।” विवेक ने सिर झुका लिया—
“माँ… अभी वक्त नहीं है…” लेकिन किस वक्त का इंतज़ार कर रहा था विवेक। वो वक्त जब उसके पास इज़्ज़त होगी, ज़ेब में तनख्वाह होगी या जब उसका दर्द सरकार की दीवारों से टकराकर वापस न लौटे।
गाँव के लोग कहते— “सरकारी नौकरी वाला बेटा है सरस्वती का… फिर भी घर में चूल्हा ठंडा है।”
“मोटरसाइकिल है फिर भी बहन के लिए चूड़ी नहीं ला सका।”
लेकिन कोई नहीं जानता था— वो मोटरसाइकिल भी किस्तों पर थी और पेट्रोल 50 रूपए से ज्यादा का कभी डलवाया नहीं गया। स्कूल के दिनों में कभी जिन दोस्तों के साथ बैठकर सपने देखता था,
अब वो कॉल भी नहीं उठाते।
एक बार एक दोस्त ने कहा था— “विवेक, तू कहीं पैसे उधार माँगने न लग जाए… इसीलिए बात नहीं करता।”
उस रात विवेक माँ की दवा लेने शहर नहीं गया। बस बहन के लिए एक सस्ती चूड़ियों का सेट खरीद लाया। घर लौटा तो माँ मुस्कुरा दी—
“बेटा, तू हमेशा कुछ न कुछ कर ही लेता है…”
फिर देर रात, जब सब सो चुके थे, विवेक की नींद… मानो कोसों दूर हो वह मन-ही-मन सोचता, कि वह… गाँव का सरकारी अफ़सर है, पर ज़ेब से फ़कीर।
विवेक रोज़ लड़ता है— रोटी से, दुनिया से, और ख़ुद की नज़रों से…
अध्याय 5 – अधिकारों की चाह, सम्मान की प्यास
सुबह के नौ बज चुके थे। विवेक ने सफेद कमीज़ पर हल्का-सा इस्त्री फेरकर अपना बैग उठाया, जिसमें गाँव की बीते छः महीने की मनरेगा, आवास योजना, शौचालय, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और वृद्धावस्था पेंशन की फाइलें ठूँसी पड़ी थीं। आज फिर ब्लॉक ऑफिस जाना है… सचिव जी ने सुबह-सुबह ही कॉल कर दी है।
दोपहर की चिलचिलाती धूप में, टीवीएस स्पोर्ट की पुरानी मोटर साइकिल स्टार्ट करते हुए, विवेक के चेहरे पर अफ़सर जैसी गंभीरता थी और एक मज़दूर जैसा पसीना।
ब्लॉक ऑफिस में भीड़ थी— ग्राम प्रधान, सचिव, एडीओ, बीडीओ साहब और उनके बाबू… सबकी एक दूसरे से पहचान थी, परिचय था— सिर्फ विवेक को कोई नहीं जानता। न कोई कुर्सी मिली, न एक गिलास पानी, वह अपने कागज़ सौंपकर घंटों लाइन में खड़ा रहा क्योंकि वह “पंचायत सहायक” था। सबसे नीचे, सबसे अदृश्य।
सचिव रमेश दुबे ने तीखे स्वर में कहा— “विवेक ! अगर ब्लॉक का कोई भी कार्य पेंडिंग रहा, तो तेरे ही खिलाफ नोटिस आ जाएगा। आज आवास की तीसरी किस्त भी फीड करनी है और हाँ, एसडीएम साहब के दौरे की तैयारी भी…”
विवेक बस सिर हिलाता रहा जैसे अफ़सर नहीं कोई मज़दूर हो— पर मजबूरी थी, इसलिए चुप रहा।
एक कंप्यूटर पर सौ काम थे उसके हिस्से। शौचालय निर्माण की ऑनलाइन फीडिंग, मनरेगा के मजदूरों की उपस्थिति, प्रधान और सचिव के यात्रा भत्ते की फाइलें, पास हुए आवासों की सूची, जनसेवा केंद्र का संचालन, मतदाता सूची में नये नाम जोड़ना, ग्राम सभा का वीडियो बनाकर अपलोड करना व बीडीओ साहब की रिपोर्टिंग… और बदले में?
न तनख्वाह, न नौकरी के स्थायित्व की कोई गारंटी वस एक संविदा कर्मचारी।
कभी-कभी लगता जैसे वह नौकरी नहीं कर रहा बल्कि किसी अंतहीन भूलभुलैया में खुद को घसीट रहा हो।
एक दिन ब्लाक में बीडीओ साहब ने ताना मारा—
पंचायत सहायक क्या होता है? डाटा एंट्री ऑपरेटर…. पूरे ऑफिस में ठहाका गूँज उठा… विवेक चुपचाप अपना बैग बंद करता रह गया, उसका मन भीतर ही भीतर कुछ कह रहा था।
“मैं गाँव का अफ़सर कहलाता हूँ लेकिन यहाँ तो कोई पहचान भी नहीं है मेरी… जिस कुर्सी पर बैठता हूँ, वो भी मेरी नहीं है और जिस फाइल पर दस्तखत करता हूँ उसका फैसला भी कोई और करता है।”
शाम होते-होते जब वो ब्लॉक से बाहर निकला, उसकी आँखों में थकान से ज़्यादा खालीपन था। सड़क से गुजरती चमचमाती कारों को देखकर सोचता—
“कितना अच्छा होता, अगर मेरी भी नौकरी ऐसी होती— एक पहचान, एक तनख़्वाह, और थोड़ी-सी इज़्ज़त।”
पर वो तो पंचायत सहायक था— जो नौकरी से ज़्यादा, व्यवस्था की सहनशीलता से बँधा हुआ और फिर… एक चुप्पी के साथ, विवेक ने खुद से कहा—
“मेरा युद्ध सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, इज़्ज़त के लिए है, जहाँ तन्ख़्वाह कम, मगर ज़ख़्म बेइन्तिहा मिलते हैं…”
अध्याय 6 – एक अधूरी मोहब्बत की वापसी
सुबह के सात बज चुके थे। सूरज अपनी किरणें फैला रहा था और विवेक पंचायत भवन जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसका बैग तैयार था— फाइलों, आवेदनों और सरकारी हुक्मनामों से भरा हुआ, हर दिन की तरह आज भी वह अपनी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधो पर लादने जा रहा हो।
किचन से रोटी की हल्की-सी खुशबू आ रही थी। चाँदनी भी माँ का हाथ बटा रही थी। हर सुबह की तरह यह सुबह भी सामान्य ही लग रही थी पर तभी—
घर में टेबल पर रखा फोन अचानक बज उठा…
ट्रिंग ट्रिंग… ट्रिंग ट्रिंग…
चाँदनी ने फोन उठाया—
हेलो…..
दूसरी ओर से एक धीमी, काँपती हुई आवाज़ सुनाई दी—
“विवेक… है?”
चाँदनी थोड़ा चौंकी…
“भैया ! आपके लिए कानपुर से किसी का फ़ोन है… लड़की है, नाम नहीं बताया…”
विवेक के हाथ से चाय का कप लगभग छूट गया, उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया हो। उसने काँपते हाथों से फोन उठाया—
हेलो…..
हैलो विवेक…..
बस दो शब्द… और जैसे समय वहीं थम गया। कमरे की हवा रुक गई, दिल की धड़कनें पुराने स्कूल की घंटी जैसी सुनाई देने लगी। उस आवाज़ में वो कँपकँपी थी, जो वर्षों बाद किसी पुराने ज़ख्म के सहलाए जाने से आती है।
नेहा… उसने काँपती आवाज़ में कहा।
हाँ…..बहुत साल बाद… लेकिन दिल अब भी वहीं है… जहाँ छोड़ा था।
…और उस पल, जैसे सब कुछ लौट आया हो—
वो स्कूल के दिन… वो प्यारी बातें…
आखिरी परीक्षा का दिन… नेहा की आँखें…
नेहा— “विवेक, तुमने एक बार भी पलटकर नहीं देखा… मैं इंतज़ार करती रही… हर उस दिन… जब तुम्हारा नाम मेरी साँसों में गूँजता था…”
फोन पर मौन की एक लंबी रेखा खिंच गई थी। काँच जितनी पारदर्शी, पर उतनी ही नुकीली।
नेहा ने धीरे से कहा—
पापा अब मान गए हैं विवेक… उन्होंने कहा है “अगर लड़का नौकरी में हो— भले ही छोटी हो, रिश्ता हो सकता है…”
विवेक ने होंठ भींचते हुए कहा—
“नेहा, पंचायत सहायक की नौकरी को, नौकरी नहीं मानते लोग… और मैं अब भी खुद को पाल नहीं पाता…”
नेहा की आवाज़ में कोई शिकायत नहीं थी— बल्कि वो सच्चाई थी जो आँखों से नहीं, सीधा दिल से निकलती है—
“मैंने तुम्हें तुम्हारी नौकरी के लिए नहीं चाहा था, विवेक…
मैंने तो तुम्हें चाहा था, तुम्हारे होने के लिए…” विवेक की आँखों से आँसू निकलकर गालों तक पहुँच चुके थे, बिना आवाज़ किए, बिना रोए…
बस यूँ ही बहते हुए, जैसे कोई बीते हुए पल वापस माँग रहा हो।
उसने धीरे से कहा— “मैं तुम्हें अपना नाम तो दे सकता हूँ, नेहा… लेकिन शायद ज़िंदगी नहीं…”
फोन पर दोनों तरफ़ चुप्पी छा गई थी।
एक ऐसी खामोशी जो शब्दों से ज़्यादा कुछ कह जाती है। शायद दोनों की रूहें ही बात कर रही थीं— वो बातें, जो कभी कह नहीं पाए थे।
फोन कटने से ठीक पहले नेहा ने कहा— “मैं तुम्हें फिर से कॉल करूँगी… उसी नंबर पर— जिस पर तुमने आखिरी बार ‘बाय’ कहा था।”
विवेक की आवाज़ जैसे किसी पुराने बक्से में रखे खत जैसी फड़फड़ाई—
“मै इंतजार करूँगा, मैं आज भी वहीं हूँ नेहा… वक़्त के पीछे… बस तुम्हारी आवाज़ के इंतज़ार में…”
फोन कट गया।
विवेक की नजर सामने दीवार पर टँगी उसी पुरानी तस्वीर पर पड़ी— नेहा अब भी मुस्कुरा रही थी… पर इस बार उसकी मुस्कान के पीछे एक सवाल था— “क्या मोहब्बत सिर्फ चुप रहने से पूरी हो जाती है?”
वो तस्वीर अब फ्रेम में नहीं थी, वो आँखों के अंदर उतर आई थी और शायद वहीं रह गई थी… हमेशा के लिए।
“नेहा की कॉल कोई संयोग नहीं थी—वो मोहब्बत की आखिरी दस्तक थी, जिसे विवेक अब भी दरवाज़े तक जाकर खोल नहीं पा रहा था।
अध्याय 7 – सीधे रास्ते की सबसे बड़ी सजा
रात के 7 बजे थे। ब्लॉक परिसर में बने छोटे से कमरे में… वहीं एक पुरानी, टूटी-सी घूमने वाली कुर्सी पर बलबीर सिंह बैठा था— हाथ में सिगरेट, चेहरे पर शिकन और मन में भय। उसके सामने खड़े थे सचिव रमेश दुबे।
“अब बहुत हो गया यह विवेक की ईमानदारी का नाटक…” बलबीर ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, “ज्यादा सीधा आदमी अगर गाँव में इज्ज़त पाने लगे, तो हमारे जैसे लोगों की नेतागीरी का क्या होगा?”
वो जानता था— पंचायत सहायक विवेक अब गाँव वालों के बीच लोकप्रिय हो चुका है लोग उसकी कार्यशैली से बहुत प्रसन्न थे। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने विवेक की बात को प्रधान से ऊपर माना।
“कल को यही लड़का अगर गाँव का प्रधान बन गया तो?” उसका दिल काँप गया था।
अब तुम ही बताओ, रमेश भैया, बलबीर एक ही साँस में बोला — “अगर गाँव वालों को जनसुनवाई, RTI, IGRS, 1076 जैसी चीज़ों की जानकारी हो गई, तो हमारी तो कहानी खत्म हैं !”
सचिव चुप थे, लेकिन अंदर ही अंदर सहमत भी क्योंकि प्रधान को जो हिस्सा मिलता था, उसी से सचिव का भी हिस्सा बनता और यही हिस्सेदारी ऊपर तक जाती थी।
बलबीर— इस बार चुनाव में 15 लाख फूँक चुका हूँ अब अगर ये पंचायत सहायक हमारे कामों में टाँग अड़ाएगा, तो भूखा मरना पड़ेगा हमें।
अध्याय 8 – सच के साए में अकेला— विवेक
प्रधान और सचिव ने मिलकर एक चाल चली— स्वच्छ भारत मिशन फेज़-2 के तहत आने वाले शौचालय निर्माण की एक नयी सूची बनाई गई। उसमें अपात्र लोगों के नाम डाले गए, जिन्हें 12,000 रुपये प्रति लाभार्थी मिलने थे।
“कागज़ पर शौचालय बनाओ, पैसे बाँटो, और असली लाभार्थी को भनक भी ना लगे।” सभी फ़र्ज़ी दस्तावेज़ तैयार हुए। अब बस विवेक के दस्तख़त चाहिए थे। वही दस्तख़त, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।
विवेक के सामने जब स्वच्छ भारत मिशन फेज़-2 शौचालय की नयी सूची आई तो वह देखते ही भौचक्का रह गया। एक-एक नाम, एक-एक दस्तावेज़ उसमे फ़र्ज़ी लगा था।
नियमावली के अनुसार सभी अपात्र थे। किसी के घर पहले से पक्का शौचालय था तो कोई गाँव में ही नहीं रहता। सूची में ऐसे लोगो के नाम थे।
विवेक— मैं इस पर दस्तख़त नहीं कर सकता, बलबीर भैया … ये गलत है।
बलबीर की आँखों में खून उतर आया….
“तेरे जैसे पंचायत सहायक बहुत देखे हैं ! ये घोटाला नहीं, सरकारी सिस्टम है, तू मुझे सिखाएगा, काम कैसे करना है। ज्यादा गाँधी मत बन ! वरना… “तू तो गया बेटे… तेरी नौकरी गई समझ।”
विवेक ने सिर झुका लिया— झुका तो जरूर, पर दस्तख़त नहीं किया।
दो दिन बाद सूचना बोर्ड पर एक गुमनाम शिकायत चिपकी मिली— “पंचायत सहायक विवेक के द्वारा अपात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है। उसे पद से निलंबित किया जाए।” प्रधान और सचिव दोनों ने मौखिक रूप से इसका समर्थन किया।
विवेक जब घर पहुँचा तो माँ सरस्वती देवी ने पूछा— “बेटा, कुछ परेशान लग रहा है… सब ठीक है?”
विवेक मुस्कुरा दिया— कुछ नहीं माँ, पंचायत घर का जरूरी काम है और चुपचाप अपने कमरे में चला गया।
उस रात उसे नींद नहीं आई। वो लेटा रहा, करवटें बदलता रहा— सोचता रहा कि जब कोई छात्र अपने कॉलेज की रातों में जागकर सपने बुनता है, देश सेवा की कसमें खाता है तो कैसे वही छात्र एक दिन अधिकारी बनते ही भ्रष्ट हो जाता है?
उसके उच्च अधिकारी, ये वही लोग हैं जो कभी खुदको देशभक्त कहते थे… फिर इनके भीतर इतना लालच कैसे आ गया, क्या वाकई सरकारी कुर्सी इंसान को बदल देती है?
वो जानता था कि उसकी यह लड़ाई सिर्फ कुर्सी की नहीं, ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो सरकारी व्यवस्था को अपने स्वार्थ की चीज़ मान चुकी है। “क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है?” वो रात भर रोता रहा वस यही सब सोच-सोच कर।
अध्याय 9 – पर्दे के पीछे की ग्राम पंचायत
सुवह के लगभग ग्यारह बजे थे। पंचायत भवन में आज ग्राम सभा की मासिक बैठक थी। छत पर पंखा घूँ-घूँ कर रहा था, मगर गर्मी की लहरें किसी लोकल नेता की तरह सब पर हावी थीं। बरामदे में गाँव के कुछ लोग चुपचाप बैठे थे— कोई सिर पर गमछा बाँधे, कोई कुर्सी की मुरमुराहट से ऊबता हुआ।
हॉल के भीतर प्रधान बलबीर सिंह अपनी कुर्सी पर ऐसे जमे थे, जैसे यही विधानसभा हो। बगल में सचिव रमेश दुबे बैठे थे— हाथ में फाइल और चेहरा तटस्थ। थोड़ी दूरी पर बैठा था विवेक— पंचायत सहायक। उसके हाथों में काग़ज़ों की गठरी थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें।
औपचारिक बातचीत चल रही थी पर भीतर कुछ और ही पक रहा था।
प्रधान बलबीर सिंह ने धीरे से झुककर कहा— “विवेक ! इस बार सचिव रमेश के कहने पर इन 12 नामों को आवास लिस्ट में जोड़ दे… सब अपने ही लोग हैं।”
जैसे ही लिस्ट देखी… एक बार फिर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सभी नाम पक्के मकान वालों के थे या फिर शहर में रहने वालों के।
उसने धीमे से लेकिन साफ़ स्वर में कहा सचिव सर—
“सर… ये सब अपात्र हैं। नियमों के अनुसार इन्हें शामिल नहीं किया जा सकता।”
बलबीर सिंह का चेहरा लाल पड़ गया। आँखों में धधकता हुआ रोष उमड़ पड़ा।
“तू पंचायत सहायक है या कोई अफ़सर बन गया है? बहुत उड़ने लगा है रे ! बस एक दस्तख़त…और तेरी ये नौकरी गई समझ।” प्रधान ने धमकी देते हुए कहा।
विवेक कुछ नहीं बोला, पर उसकी पीठ पसीने से भीग गई थी। भीतर एक कँपकँपी थी— न डर की, बल्कि व्यवस्था की निर्ममता को जानने की।
उस रात सचिव का फोन आया। “देखो विवेक, बात समझो। प्रधान से उलझना बेवकूफी है। सब सिस्टम से समझौता करते हैं। तुम भी कर लो वरना ये नौकरी भी हाथ से जाएगी।”
विवेक चुप रहा। काफी देर तक कमरे की दीवारों को घूरता रहा, फिर डायरी खोली और माँ की कही बात याद आई— “गलत को गलत कहना कभी मत छोड़ना।”
कुछ ही हफ्तों में चीज़ें तेज़ी से बदलीं। जिला DPRO कार्यालय में विवेक के नाम शिकायत पहुँची— “काम में लापरवाही”
एक नोटिस आया— “कारण बताओ नोटिस”
गाँव में अफवाह फैली— “विवेक रिश्वत लेता है…”
एक-एक कदम जैसे किसी तयशुदा साज़िश का हिस्सा था। वह घिर चुका था— सत्ता, सिस्टम, और साजिश के त्रिकोण में। उधर बलबीर सिंह अब भी ऐसे हँसता था जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
गाँव वाले भी अब विवेक से आँखें चुराते थे और सचिव रमेश दुबे, जो कभी सहयोगी लगते थे, अब अजनबी हो गए थे। विवेक के पास न कोई नेता था, न पैसे का सहारा। न कोई जातिगत ढाल, न कोई अधिकारी जो उसका पक्ष ले। बस उसके साथ था— उसका सच, उसका संघर्ष, और उसकी माँ का आशीर्वाद।
उस दिन अकेले बैठकर उसने खुद से कहा—
“जिस व्यवस्था को सँवारने की मैंने कसम खाई थी, अब वही मुझे तोड़ने को आमादा है। क्या ईमानदारी सच में बस किताबों की कहानी है?”
उसकी आँखें नम थीं, पर उनमें कोई पछतावा नहीं था। वह डरा हुआ था… लेकिन अब भी टूटा नहीं था।
अध्याय 10 – लखनऊ की सुबह और गाँव की आवाज़
सुबह के चार बजे थे। अलार्म की घड़ी तो बजी नहीं, पर विवेक की आँखें यूँ ही खुल गईं। जैसे शरीर सो भी जाए, तो भी आत्मा को चैन कहाँ। उसने कितनी ही रातें ऐसे ही करवटों में गुज़ार दी थीं—
न नींद थी, न सुकून… बस एक अदृश्य लड़ाई चल रही थी— एक अदृश्य सिस्टम के खिलाफ।
आज उसे राजधानी जाना था। लखनऊ न्याय की तलाश में अपने जैसे हजारों पंचायत सहायकों की आवाज़ बनकर।
वो अकेला नहीं था— प्रदेश भर के कोनों से आये पंचायत सहायक भी वही दर्द लिए थे— अधूरी सच्चाइयों के गवाह।
“हम तनख़्वाह नहीं, इज़्ज़त माँगने आए हैं… “बस अड्डे की चाय की दुकान पर बैठा विवेक, हाथ में लिए अपनी नियुक्ति पत्र की प्रति और अनुभव पत्रों को एकटक देख रहा था। हर काग़ज़ उसकी मेहनत की कहानी कहता था।
वह पंचायती राज निदेशालय के सामने पहुँचा— हज़ारों पंचायत सहायकों के बीच। किसी के हाथ में पोस्टर, किसी की आँखों में उम्मीदें और सभी के सीने में जले हुए सपने।
“हम भी कर्मचारी हैं— मान्यता दो, हमें स्थायी करो !”
“20 घंटे काम, 8 घंटे की तनख़्वाह भी नहीं !”
“पंचायत सहायक नहीं, पंचायत का मज़दूर बना दिया !”
भीड़ थी— लेकिन अनुशासित।
आवाज़ें थीं— लेकिन सलीकेदार। कोई नारे लगा रहा था, कोई बस खामोशी में भीग रहा था।
तभी एक पत्रकार आया— युवा, ईमानदार, जिज्ञासु। विवेक के पास आकार कैमरा ऑन किया।
“आपका नाम?”
“विवेक। गाँव— रामपुरा, पंचायत सहायक।”
“कितने साल से काम कर रहे हो?”
“चार साल, अभी तक स्थायी नहीं हुआ।”
“आप क्या चाहते हैं?”— पत्रकार ने पूछा।
विवेक ने सीधे कैमरे में देखा, उसकी आवाज़ धीमी थी पर असरदार— “बस यही चाहता हूँ कि जब सरकार हमें अफ़सरों जैसा काम देती है, तो तनख़्वाह और सम्मान भी वैसा ही दे। सिर्फ छः हजार में घर कैसे चलायें। हम गाँव के अफ़सर हैं… पर ज़ेब के फकीर। यही है हमारी कहानी— पंचायत सहायक, गाँव का अफ़सर, ज़ेब का फकीर— एक अधूरी सच्चाई।”
उस वीडियो ने जैसे आग लगा दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ—
लोग कहने लगे— “गाँव का लड़का सरकार से टकरा गया।”
अगले ही दिन, राज्य सचिवालय से बुलावा आया।
अपने कुछ साथियों के साथ, विवेक पंचायती राज विभाग के निदेशक से मिलने गया। दफ्तर में बैठे अधिकारी ने कहा— “हमने आपकी बातें सुनी हैं, विवेक। हम प्रस्ताव बनाएँगे। कमेटी गठित होगी। जो हो सकेगा, किया जाएगा…”
विवेक बाहर आया—
दिल में सुकून नहीं था लेकिन चेहरे पर शांति ज़रूर थी।
“शायद बात पहुँची है… शायद नहीं। लेकिन आज हमने एक शुरुआत की है और यही सबसे बड़ी जीत है।”
गाँव लौटते वक़्त, बस की खिड़की से बाहर झाँकते हुए, उसने मोबाइल में नेहा का मैसेज पढ़ा—
“मुझे माफ़ करना विवेक, मुझे तुम पर हमेशा गर्व था। तुम नहीं बदले, क्योंकि तुम झुके नहीं।”
विवेक की बहन चाँदनी बस अड्डे पर विवेक को लेने आयी— “भैया, आज माँ बहुत खुश है। टीवी पर तुम्हारी फोटो आ रही थी। सब कह रहे थे— ‘देखो गाँव का लड़का कितना बड़ा हो गया’।”
विवेक मुस्कराया नहीं— बस आंखें थोड़ी भर आईं।
घर आया और कमरे में पहुंचा तो देखा दीवार पर अब भी वही पुराना कैलेंडर टँगा था पर तारीख़ बदल चुकी थी।
एक नया दिन… एक नयी शुरुआत। वो बैग अब भी कंधे पर था लेकिन आज वो बोझ नहीं लग रहा था। जैसे सालों की मेहनत ने आज उसे कुछ और बना दिया हो— एक आंदोलन का चेहरा, एक उम्मीद का नाम।
वह अधूरी सच्चाई अब आंदोलन का रूप ले चुकी थी। अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर विवेक ने लिखा—
“जिसने गाँव के लिए कलम चलाई, आज उसकी आवाज़ राजधानी तक पहुँची। तनख़्वाह भले न बढ़ी हो, पर समाज की नज़र में अब ‘पंचायत सहायक’ सिर्फ नाम नहीं, सम्मान है और मैं जानता हूँ—
मुश्किलों से निकली हुई सच्चाई कभी अधूरी नहीं रहती। धीरे-धीरे ही सही, समाज को उसे स्वीकारना ही पड़ता है।
साथियों, यह उपन्यास पंचायत सहायकों की असली पीड़ा की आवाज़ है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि समाज और सरकार तक पंचायत सहायकों की आवाज़ पहुँचे। हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही पंचायत सहायकों के हित में भारत सरकार कोई सकारात्मक कदम उठाएगी। पंचायत सहायक लेखक सतेन्द्र का यह पहला उपन्यास है — पंचायत सहायकों के हित में इस ऐतिहासिक रचना को लिखने के लिए हम उन्हें एक बार पुनः दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
धन्यवाद युवा लेखक सतेन्द्र जी